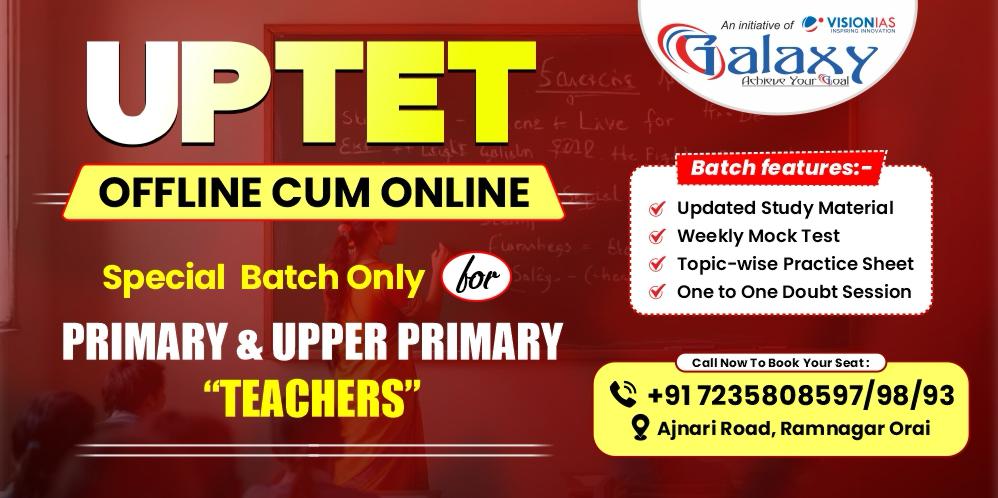08 December, 2025
चार श्रम संहिताएं लागू
Mon 24 Nov, 2025
संदर्भ :
- केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को आसान और कारगर बनाने के उद्देश्य से 21 नवंबर, 2025 से चार श्रम संहिताओं को लागू किया, जिसके माध्यम से 29 वर्तमान श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित किया जाएगा ।
संहिताएं :
- वेतन संहिता, 2019 : मजदूरी, न्यूनतम वेतन, बोनस और समान पारिश्रमिक से सम्बन्धित
- औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 : ट्रेड यूनियन, औद्योगिक विवादों के समाधान, और काम की स्थायी व्यवस्था से संबंधित
- सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 : कर्मचारी भविष्य निधि (PF), कर्मचारी राज्य बीमा (ESI), ग्रेच्युटी, मातृत्व लाभ और पेंशन से संबंधित
- व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 : कार्यस्थल पर सुरक्षा, स्वास्थ्य और कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित
अधिसूचित :
- वेतन संहिता, 2019 को 8 अगस्त, 2019 को और शेष तीन संहिताओं को 29 सितंबर, 2020 को
वेतन संहिता, 2019:
- लक्ष्य : भारत के श्रम कानूनों में सुधार लाना
- यह चार पुराने कानूनों के प्रावधानों को सरल और एकीकृत करती है, जिससे श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके और साथ ही, नियोक्ताओं के लिए अनुपालन (Compliance) आसान हो सके।
समाहित किए गए पूर्ववर्ती कानून :
- मजदूरी भुगतान अधिनियम, 1936
- न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948
- बोनस भुगतान अधिनियम, 1965
- समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976
मुख्य उद्देश्य :
- श्रमिकों का सशक्तीकरण: वेतन और बोनस के संदर्भ में सभी श्रमिकों के अधिकारों को सुदृढ़ करना।
- अनुपालन में सरलता: नियोक्ताओं के लिए वेतन संबंधी नियमों के पालन में एकरूपता और सरलता लाना
प्रमुख प्रावधान और विशेषताएँ
सार्वभौमिक न्यूनतम वेतन का अधिकार :
- यह संहिता संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों के सभी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन के वैधानिक अधिकार को सर्वव्यापी बनाती है।
- पूर्व स्थिति: इससे पहले, न्यूनतम वेतन अधिनियम केवल विशिष्ट "अनुसूचित रोजगारों" पर लागू होता था, जो श्रमबल के एक छोटे हिस्से को ही कवर करता था।
वैधानिक राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन (Floor Wage) :
- केंद्र सरकार देश भर में श्रमिकों के न्यूनतम जीवन स्तर पर आधारित एक वैधानिक न्यूनतम वेतन (जिसे 'फ्लोर वेज' कहा जाता है) निर्धारित करेगी, जिसमें क्षेत्रीय विषमताओं को ध्यान में रखा जा सकता है।
- राज्यों पर बाध्यता: किसी भी राज्य सरकार को यह अनुमति नहीं होगी कि वह अपने क्षेत्र में इस राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन से कम न्यूनतम वेतन निर्धारित करे, जिससे देश भर में मजदूरी की पर्याप्तता और एकरूपता बनी रहे।
ओवरटाइम के लिए मुआवजा :
- यदि कोई कर्मचारी नियमित कार्य घंटों से अधिक काम करता है, तो नियोक्ता को उस कार्य के लिए सामान्य मजदूरी दर से कम-से-कम दोगुना वेतन देना अनिवार्य है।
अपराधों का गैर-अपराधीकरण :
- यह कानून कुछ पहली बार किए गए छोटे उल्लंघनों के लिए जेल भेजने (कारावास) के प्रावधान को समाप्त करता है।
- इसके बजाय, इसमें मौद्रिक जुर्माने (अधिकतम जुर्माने के 50% तक) का प्रावधान किया गया है। यह ढाँचा दंडात्मक होने के बजाय अनुपालन को प्रोत्साहित करने वाला बनाया गया है।
औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 :
- प्राथमिक उद्देश्य: ट्रेड यूनियनों, औद्योगिक उपक्रमों में रोजगार की शर्तों और औद्योगिक विवादों के समाधान से संबंधित मौजूदा श्रम कानूनों को सरल, एकीकृत और तर्कसंगत बनाना है।
समाहित किए गए पूर्ववर्ती कानून :
- ट्रेड यूनियन अधिनियम, 1926
- औद्योगिक रोज़गार (स्थायी आदेश) अधिनियम, 1946
- औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947
मुख्य प्रावधान और नवाचार
श्चित अवधि का रोजगार (Fixed Term Employment - FTE) :
- यह संहिता निश्चित समय-सीमा के लिए प्रत्यक्ष अनुबंधों के आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देती है।
- समानता सुनिश्चित: इन FTE कर्मचारियों को नियमित कर्मचारियों के समान वेतन, भत्ते और लाभ (जैसे वैधानिक अवकाश) प्राप्त होंगे।
- ग्रेच्युटी पात्रता: FTE कर्मचारी एक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद ही ग्रेच्युटी के हकदार बन जाते हैं।
- लाभ: यह प्रावधान अत्यधिक संविदाकरण की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करता है, जबकि नियोक्ताओं को परिचालन लचीलापन प्रदान करता है
कर्मचारियों के लिए पुनः कौशलीकरण निधि (Reskilling Fund) :
- उद्देश्य: छंटनी (retrenchment) किए गए कर्मचारियों को नए कौशल सिखाने और उन्हें पुनः प्रशिक्षित करने के लिए एक समर्पित निधि की स्थापना की गई है।
- नियोक्ता अंशदान: प्रत्येक औद्योगिक प्रतिष्ठान को प्रत्येक छंटनी किए गए कर्मचारी के लिए 15 दिनों के वेतन के बराबर राशि इस निधि में जमा करनी होगी।
ट्रेड यूनियन की मान्यता और वार्ता प्रक्रिया :
- वार्ताकार संघ: किसी ट्रेड यूनियन को एकमात्र वार्ताकार संघ (Negotiating Union) के रूप में मान्यता तभी मिलेगी जब उसकी सदस्यता प्रतिष्ठान के कम-से-कम 51% श्रमिकों में होगी।
- वार्ता परिषद: यदि कोई भी यूनियन 51% सदस्यता प्राप्त नहीं करती है, तो कम-से-कम 20% सदस्यता वाले यूनियनों से मिलकर एक वार्ता परिषद का गठन किया जाएगा।
- लाभ: यह संरचना सामूहिक सौदेबाजी की शक्ति को मजबूत करती है।
शीघ्र विवाद निपटान के लिए न्यायाधिकरण :
- दो सदस्यीय न्यायाधिकरण: शीघ्र विवाद समाधान के लिए न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों से युक्त दो सदस्यीय औद्योगिक न्यायाधिकरणों की स्थापना का प्रावधान है।
- सीधी पहुँच: सुलह की प्रक्रिया विफल होने पर, विवाद के पक्षकार अब 90 दिनों के भीतर सीधे इन न्यायाधिकरणों से संपर्क कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया में तेजी आती है।
हड़ताल और तालाबंदी के लिए अनिवार्य सूचना :
- 14 दिन का नोटिस: सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में किसी भी हड़ताल (Strike) या तालाबंदी (Lock-out) को शुरू करने से पहले 14 दिन का अनिवार्य नोटिस देना आवश्यक है। इसका उद्देश्य अंतिम उपाय के रूप में कार्रवाई करने से पहले बातचीत और सुलह के लिए पर्याप्त समय देना है।
- हड़ताल की व्यापक परिभाषा: अचानक और अनियोजित कार्य-स्थगन को रोकने के लिए, "सामूहिक आकस्मिक अवकाश" को भी हड़ताल की परिभाषा के दायरे में शामिल किया गया है।
महिला कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व :
- शिकायत निवारण समिति: संहिता में लैंगिक रूप से संवेदनशील मामलों को प्रभावी ढंग से हल करने के लिए शिकायत निवारण समितियों में महिलाओं का आनुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।
सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 :
- उद्देश्य : भारत में सामाजिक सुरक्षा लाभों के वितरण को व्यापक और सरल बनाना
- समाहित किए गए पूर्ववर्ती सामाजिक सुरक्षा कानून :
कुल नौ (9) मौजूदा केंद्रीय सामाजिक सुरक्षा अधिनियमों के प्रावधानों को समेकित करती है -
- कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम, 1923
- कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948
- कर्मचारी भविष्य निधि एवं विविध प्रावधान अधिनियम, 1952
- रोजगार कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम, 1959
- मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961
- उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 (ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972)
- सिनेमा-कर्मचारी कल्याण निधि अधिनियम, 1981
- भवन एवं अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996
- असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम, 2008
मुख्य नवाचार और विस्तार
- गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों का समावेशन :
- यह संहिता असंगठित क्षेत्र, साथ ही गिग और प्लेटफॉर्म कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाती है, जो पहले औपचारिक सुरक्षा से वंचित थे।
- नई परिभाषाएँ: इसमें 'एग्रीगेटर', 'गिग कर्मचारी' और 'प्लेटफॉर्म कर्मचारी' जैसे नए कामकाजी मॉडलों को परिभाषित किया गया है ताकि उन्हें कानूनी कवरेज मिल सके।
- योगदान तंत्र: इन कर्मचारियों को लाभ देने वाली योजनाओं के लिए, एग्रीगेटर अपने वार्षिक कारोबार का 1% से 2% तक का योगदान करेंगे (हालांकि यह राशि इन कर्मचारियों को दिए गए भुगतान के 5% से अधिक नहीं होगी)।
विस्तारित ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) कवरेज :
- देशव्यापी कार्यान्वयन: ESIC योजना अब पूरे भारत में लागू होती है, जिससे पहले लागू होने वाले 'अधिसूचित क्षेत्रों' की भौगोलिक बाध्यता समाप्त हो जाती है।
- स्वेच्छा से शामिल होने का प्रावधान: 10 से कम कर्मचारियों वाले छोटे प्रतिष्ठान भी, नियोक्ता और कर्मचारियों की आपसी सहमति से, ESIC योजना में स्वेच्छा से शामिल हो सकते हैं।
'वेतन' की एकरूप परिभाषा :
- समान आधार: संहिता 'वेतन' की एक समान परिभाषा स्थापित करती है, जिसमें मूल वेतन, महँगाई भत्ता और प्रतिधारण भत्ता (Retaining Allowance) शामिल है।
- सीमा निर्धारण: यदि किसी कर्मचारी को मिलने वाला भत्ते वाला भाग (अलाउंस) उसके कुल पारिश्रमिक के 50% से अधिक हो जाता है, तो उस अतिरिक्त राशि को भी वेतन की गणना में जोड़ा जाएगा।
- लाभ: यह एकरूपता ग्रेच्युटी, भविष्य निधि (PF) और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभों की गणना में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है।
निश्चित अवधि के रोजगार के लिए ग्रेच्युटी :
- निश्चित अवधि के अनुबंध (FTE) पर काम करने वाले कर्मचारी अब एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद ही ग्रेच्युटी के लिए पात्र हो जाते हैं। (पहले यह पात्रता पाँच वर्ष की निरंतर सेवा के बाद मिलती थी)।
EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) जाँच में समयबद्धता :
- जाँच की समय-सीमा: EPF संबंधी जाँच (Inquiry) और वसूली की कार्यवाही शुरू करने के लिए पाँच वर्ष की समय-सीमा निर्धारित की गई है।
- अनिवार्य समापन: एक बार कार्यवाही शुरू होने के बाद, उसे दो वर्षों के भीतर पूरा करना अनिवार्य है, जिसे असाधारण परिस्थितियों में अधिकतम एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।
- स्वतः संज्ञान की समाप्ति: समयबद्ध समाधान की गारंटी सुनिश्चित करने के लिए मामलों के स्वतः संज्ञान (Suo Motu) संबंधी प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है।
समर्पित सामाजिक सुरक्षा निधि :
- उद्देश्य: असंगठित, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए जीवन, दिव्यांगता, स्वास्थ्य और वृद्धावस्था लाभों से संबंधित योजनाओं के वित्तपोषण के लिए एक विशेष सामाजिक सुरक्षा निधि का प्रस्ताव किया गया है।
- वित्त पोषण: विभिन्न श्रम उल्लंघनों के लिए अपराधों के शमन (Compounding of Offences) से एकत्रित राशि को इस कोष में जमा किया जाएगा, जिसका उपयोग सरकार द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए किया जाएगा।
व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशा संहिता, 2020 :
- उद्देश्य : भारत में श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करना
- यह 13 केंद्रीय श्रम कानूनों को एक व्यापक संहिता में पिरोती है।
- यह कानूनों की बहुलता को खत्म कर उद्योगों और राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के बीच एकरूपता लाती है।
समाहित किए गए 13 कानून :
- फैक्ट्रीज़ एक्ट, 1948
- प्लांटेशन लेबर एक्ट, 1951
- माइंस एक्ट, 1952
- वर्किंग जर्नलिस्ट और दूसरे न्यूज़पेपर एम्प्लॉई (सर्विस की शर्तें और मिसलेनियस प्रोविज़न) एक्ट, 1955
- वर्किंग जर्नलिस्ट (मज़दूरी की दरें तय करना) एक्ट, 1958
- मोटर ट्रांसपोर्ट वर्कर्स एक्ट, 1961
- बीड़ी और सिगार वर्कर्स (रोज़गार की शर्तें) एक्ट, 1966
- कॉन्ट्रैक्ट लेबर (रेगुलेशन और खत्म करना) एक्ट, 1970
- सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉई (सर्विस की शर्तें) एक्ट, 1976
- इंटर-स्टेट माइग्रेंट वर्कर (रोज़गार का रेगुलेशन और सर्विस की शर्तें) एक्ट, 1979
- सिने वर्कर्स और सिनेमा थिएटर वर्कर्स एक्ट, 1981
- डॉक वर्कर्स (सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर) एक्ट, 1986
- बिल्डिंग और अन्य कंस्ट्रक्शन वर्कर्स (रेगुलेशन ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशंस ऑफ़ सर्विस) एक्ट, 1996
मुख्य प्रावधान और विशेषताएँ
पंजीकरण और अनुपालन में सरलता :
- एकीकृत पंजीकरण: कई अधिनियमों के तहत छह बार पंजीकरण कराने की आवश्यकता को समाप्त करते हुए, अब एक प्रतिष्ठान के लिए एक ही इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण की व्यवस्था की गई है।
- समान सीमा: इलेक्ट्रॉनिक पंजीकरण के लिए 10 कर्मचारियों की एक समान सीमा निर्धारित की गई है।
- ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस : इससे एक केंद्रीकृत डेटाबेस बनेगा और अनुपालन में सरलता आएगी
सुरक्षा मानकों का विस्तार :
- खतरनाक कार्यों तक विस्तार: सरकार को यह अधिकार है कि वह संहिता के प्रावधानों को एक कर्मचारी वाले प्रतिष्ठानों पर भी लागू कर सकती है, बशर्ते वे खतरनाक व्यवसायों में संलग्न हों, जिससे सुरक्षा जाल को व्यापक बनाया जा सके।
प्रवासी श्रमिकों की सुरक्षा :
- व्यापक परिभाषा: अंतर-राज्यीय प्रवासी श्रमिकों (Inter-State Migrant Workers - ISMW) की परिभाषा का विस्तार किया गया है। इसमें अब ठेकेदारों के माध्यम से, सीधे या स्वयं प्रवास करने वाले सभी श्रमिक शामिल हैं।
- जवाबदेही: प्रतिष्ठानों के लिए ISMW की संख्या घोषित करना अनिवार्य कर दिया गया है।
कार्यस्थल में औपचारिकता और पारदर्शिता :
- नियुक्ति-पत्र: पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए, सभी कर्मचारियों को नियुक्ति-पत्र प्रदान करना अनिवार्य है, जिसमें नौकरी का विवरण, वेतन संरचना और सामाजिक सुरक्षा लाभों का स्पष्ट उल्लेख होगा।
महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा :
- समानता और समावेशिता: यह संहिता महिलाओं को सभी प्रकार के प्रतिष्ठानों में रोजगार की अनुमति देती है।
- रात्रि कार्य: महिलाओं को उनकी सहमति और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात के समय (सुबह 6 बजे से पहले और शाम 7 बजे के बाद) भी काम करने की अनुमति दी गई है।
राष्ट्रीय डेटाबेस और कल्याण कोष :
- असंगठित श्रमिकों का डेटाबेस: प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय डेटाबेस विकसित किया जाएगा, जो उन्हें रोजगार दिलाने, कौशल का आकलन करने और सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने में सहायक होगा।
- सामाजिक सुरक्षा कोष: असंगठित श्रमिकों के कल्याण के लिए एक समर्पित कोष स्थापित किया जाएगा, जिसका वित्तपोषण दंड और चक्रवृद्धि शुल्क (fines and compounding fees) से प्राप्त राशि से होगा।
ठेका श्रम संबंधी सुधार :
- अनुप्रयोगिता सीमा में वृद्धि: ठेका श्रमिकों की संख्या की सीमा 20 से बढ़ाकर 50 कर दी गई है, जिसके ऊपर ठेका श्रम कानून लागू होंगे।
- लाइसेंसिंग सरलीकरण: ठेकेदारों को अब कार्य-आदेश के आधार पर लाइसेंस दिए जाएंगे, जबकि अखिल भारतीय लाइसेंस 5 वर्षों के लिए वैध होगा। कुछ मामलों में लाइसेंस स्वतः 'जनरेट' होने का प्रावधान भी है।
- सलाहकारी बोर्ड का अंत: निविदा श्रम बोर्ड का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, और मुख्य तथा गौण गतिविधियों पर सलाह देने के लिए नामित प्राधिकारी की नियुक्ति की जाएगी।
कार्य समय और सुरक्षा समितियाँ :
- कार्य समय सीमा: सामान्य कार्य समय 8 घंटे प्रति दिन और 48 घंटे प्रति सप्ताह तक सीमित है।
- ओवरटाइम मुआवजा: ओवरटाइम केवल श्रमिक की सहमति से ही किया जाएगा और इसका भुगतान नियमित दर से दोगुना होगा।
- सुरक्षा समितियाँ: 500 या उससे अधिक श्रमिक संख्या वाले प्रतिष्ठानों को नियोक्ता-श्रमिक प्रतिनिधित्व वाली सुरक्षा समितियाँ बनाना अनिवार्य है, जिससे कार्यस्थल सुरक्षा में साझा जवाबदेही बढ़ेगी।
सलाहकार बोर्डों का एकीकरण :
- राष्ट्रीय सलाहकार बोर्ड: विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों में एकरूपता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पहले के छह बोर्डों का स्थान अब राष्ट्रीय व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य सलाहकार बोर्ड लेगा। यह एक त्रिपक्षीय (सरकार, नियोक्ता, श्रमिक) सलाहकार निकाय होगा।
ठेका श्रमिकों का कल्याण एवं वेतन दायित्व :
- कल्याण सुविधाएँ: प्रधान नियोक्ता ठेका श्रमिकों को स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसी कल्याणकारी सुविधाएँ प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- वेतन सुरक्षा: यदि ठेकेदार वेतन भुगतान में विफल रहता है, तो प्रधान नियोक्ता को ठेका श्रमिक को बकाया वेतन का भुगतान करना होगा।