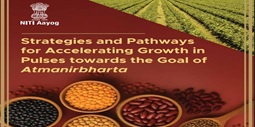21 September, 2025
"आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीतियाँ और मार्ग" नामक रिपोर्ट
Fri 05 Sep, 2025
संदर्भ :
- नीति आयोग ने "आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दलहनों के विकास में तेजी लाने की रणनीतियाँ और मार्ग" नामक रिपोर्ट जारी की है।
परिचय :
- दलहन, जो भारत की खाद्य सुरक्षा और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं।
- यह रिपोर्ट दलहन उत्पादन, प्रसंस्करण, और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करने के लिए रणनीतियों और नीतिगत सुझावों पर केंद्रित है, ताकि आयात पर निर्भरता कम हो और स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा मिले।
- इस रिपोर्ट पर नीति आयोग की वरिष्ठ सलाहकार (कृषि प्रौद्योगिकी प्रभाग) डॉ. नीलम पटेल ने प्रस्तुतिकरण दिया।
रिपोर्ट का उद्देश्य :
- भारत को दालों (दलहन) के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना और 2030 तक आत्मनिर्भरता हासिल करना तथा 2047 तक उत्पादन को दोगुना करना
वर्तमान स्थिति और प्रगति
उत्पादन और आयात:
- 2015-16 में दलहन उत्पादन 16.35 मिलियन टन (MT) था, जिसके कारण 6 एमटी आयात की आवश्यकता पड़ी।
- 2022-23 तक उत्पादन 59.4% बढ़कर 26.06 MT हो गया, और उत्पादकता में 38% की वृद्धि हुई।
- आयात निर्भरता 29% से घटकर 10.4% रह गई।
क्षेत्रीय योगदान:
- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, और राजस्थान कुल उत्पादन का ~55% योगदान करते हैं।
- शीर्ष 10 राज्य राष्ट्रीय उत्पादन का 91% से अधिक हिस्सा हैं।
- कृषि-जलवायु: भारत की विविध जलवायु खरीफ, रबी, और ग्रीष्म ऋतुओं में 12 दलहनी फसलों की खेती के लिए अनुकूल है।
- निर्भरता: दलहन उत्पादन का ~80% वर्षा आधारित क्षेत्रों पर निर्भर है, जो जलवायु जोखिमों के प्रति संवेदनशील है।
प्रमुख रणनीतियाँ
रिपोर्ट दो मुख्य स्तंभों पर आधारित रणनीतियाँ प्रस्तुत करती है: क्षैतिज विस्तार और ऊर्ध्वाधर विस्तार।
क्षैतिज विस्तार (क्षेत्रफल बढ़ाना) :
- अप्रयुक्त भूमि का उपयोग: चावल की परती भूमि और अन्य अप्रयुक्त क्षेत्रों में उच्च उपज वाली दलहन फसलों और अंतर-फसलों की खेती को बढ़ावा देना
- लक्षित फसल-वार क्लस्टरिंग: विशिष्ट क्षेत्रों में दलहन उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण, जैसे "एक ब्लॉक-एक बीज ग्राम" मॉडल
- 111 उच्च-संभावित जिले: राष्ट्रीय उत्पादन में 75% योगदान देने वाले जिलों पर विशेष ध्यान
- क्षेत्र प्रतिधारण और विविधीकरण: दलहन खेती को अन्य फसलों के साथ संतुलित करना
ऊर्ध्वाधर विस्तार (उपज बढ़ाना) :
- उन्नत किस्में और संकर: उच्च उपज और रोग-प्रतिरोधी बीजों का विकास और वितरण।
- बीज उपचार और गुणवत्ता: बीज उपचार किट और गुणवत्ता आश्वासन पर जोर
आधुनिक कृषि पद्धतियाँ:
- समय पर और वैज्ञानिक बुवाई
- पोषक तत्व, कीट, खरपतवार, और जल प्रबंधन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण
- प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप: ड्रोन, सेंसर, और AI-आधारित उपकरणों का उपयोग
- मूल्यवर्धन: प्रसंस्करण इकाइयों और भंडारण सुविधाओं का विकास
किसान सशक्तिकरण :
- FPOs (किसान उत्पादक संगठन): सामूहिक खेती और बाजार पहुँच को बढ़ावा देना
- महिला भागीदारी: ग्रामीण महिलाओं को प्रशिक्षण और सहायता
- प्राथमिक सर्वेक्षण: 5 प्रमुख राज्यों (राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक) के 885 किसानों से अंतर्दृष्टि
दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन (2025-26) :
- घोषणा: केंद्रीय बजट 2025-26 में "दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन" की शुरुआत
- अवधि: 6 वर्ष (2025-2031)
- फोकस: अरहर, काला चना, और मसूर पर केंद्रित उत्पादन बढ़ाना।
- लक्ष्य: आयात पर निर्भरता को और कम करना और घरेलू आपूर्ति को मजबूत करना
अनुमानित परिणाम
उत्पादन अनुमान:
- 2030 तक: 30.59 एमटी (रिपोर्ट का अनुमान) और 48.44 एमटी (रणनीति लागू होने पर)
- 2047 तक: 45.79 एमटी (रिपोर्ट का अनुमान) और 63.64 एमटी (रणनीति लागू होने पर)
- वृद्धि: रणनीतियों के केंद्रित कार्यान्वयन से ~20.10 एमटी की अतिरिक्त वृद्धि संभव
- आयात में कमी: आयात निर्भरता को न्यूनतम करना
- पोषण सुरक्षा: प्रोटीन युक्त दलहनों की उपलब्धता बढ़ाना
- किसान आय: बेहतर बाजार और मूल्यवर्धन से आय में वृद्धि
- पर्यावरणीय लाभ: मृदा स्वास्थ्य और जलवायु अनुकूल खेती से टिकाऊ कृषि
रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिशें:
- क्षेत्र वृद्धि: चावल की परती भूमि और अप्रयुक्त क्षेत्रों का उपयोग
- उच्च गुणवत्ता वाले बीज: बीज वितरण और उपचार किटों को बढ़ावा
- क्लस्टर-आधारित दृष्टिकोण: 111 उच्च-संभावित जिलों पर ध्यान
- FPO मॉडल: "एक ब्लॉक-एक बीज ग्राम" के माध्यम से सामूहिक खेती
- जलवायु अनुकूलन: सूखा-सहिष्णु किस्में और टिकाऊ प्रथाएँ
- डेटा-आधारित नीतियाँ: निगरानी और निर्णय-समर्थन प्रणालियों का उपयोग
- निर्यात प्रोत्साहन: गुणवत्ता मानकों को पूरा करके निर्यात बढ़ाना
नीति आयोग
- पूर्ण नाम: राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान (National Institution for Transforming India - NITI Aayog)
- मुख्यालय: नई दिल्ली
उद्देश्य:
- भारत के विकास के लिए रणनीतिक नीतियां और कार्यक्रम तैयार करना
- केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना
- नीतियों के कार्यान्वयन के लिए तकनीकी और रणनीतिक सलाह देना
- सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) को प्राप्त करने में सहायता करना
- नवाचार, उद्यमिता और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना
संरचना:
- अध्यक्ष: भारत के प्रधानमंत्री (वर्तमान में नरेंद्र मोदी)
- उपाध्यक्ष: नीति आयोग का कार्यकारी प्रमुख, जो नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन का नेतृत्व करता है (वर्तमान में सुमन बेरी)
- सदस्य: पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्य, जो विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं (उदाहरण: डॉ. वी.के. सारस्वत, डॉ. अरविंद विरमानी)
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO): दैनिक कार्यों का प्रबंधन करता है (वर्तमान में बी.वी.आर. सुब्रह्मण्यम)
- शासी परिषद: इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री शामिल हैं
प्रमुख कार्य:
- विकसित भारत@2047: भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए रणनीति तैयार करना
- नीतिगत सुधारों के लिए सुझाव देना, जैसे MSME, डिजिटल परिवर्तन, और सतत विकास
- विभिन्न क्षेत्रों जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, और बुनियादी ढांचे में नीतियां बनाना
- राज्यों के साथ मिलकर विकास परियोजनाओं को लागू करना
- डेटा-संचालित नीति निर्माण के लिए डिजिटल उपकरणों और अनुसंधान का उपयोग
प्रमुख पहल:
- आकांक्षी जिला कार्यक्रम (Aspirational Districts Programme): पिछड़े जिलों के समग्र विकास के लिए
- अटल नवाचार मिशन (Atal Innovation Mission): नवाचार और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना
- डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया: डिजिटल परिवर्तन और उद्यमिता को प्रोत्साहन
- नीति संवाद: केंद्र और राज्यों के बीच नीतिगत चर्चा के लिए मंच
- सतत विकास लक्ष्य (SDG) इंडिया इंडेक्स: राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति का मूल्यांकन